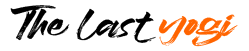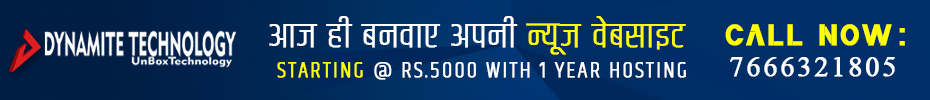गांवों में किसान भले ही कभी अखबार नहीं पढ़ते हो, परंतु मई -जून का महीना आते ही मानसून कहां पहुंचा इसकी खबर लेने को उत्सुक रहते हैं। मानसून मुख्यतः मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन है। चूंकि भारत की भौगोलिक स्थिति भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। इसलिए यहां अधिकांश वर्षा मानसून से होती हैं। सर्दी के छह महीने हवा स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मी के महीने हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यही मानसून की थर्मल कांसेप्ट है।
इस साल की शुरुआत में भारत के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि इस बार देश में सामान्य मानसून की वर्षा होने की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य में अवस्थित मौसम विभागों की रिपोर्ट में भी वार्षिक मानसून वर्षा लंबी अवधि के औसत से 98% अधिक रहने की उम्मीद जताई गयी ,जो उच्च कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास की संभावना पैदा करती है। अर्थात उच्च कृषि उत्पादन व आर्थिक विकास मानसून के प्रकार पर निर्भर करता है। चूंकि भारत पर आजादी के बाद भी औपनिवेशिक शोषण के दंश मौजूद है। हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है ,जहां अधिकांश परिवार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां गहन कृषि की जाती है और इसके चलते यहां भू जोतो का आकार सामान्यतः लघु होता है। इसी का परिणाम है कि कृषि में आवश्यक निवेश की कमी की समस्या रहती है। आज भी हमारी कृषि का लगभग 60 % हिस्सा मानसूनी वर्षा द्वारा संचित होता है । अगर कभी मानसून कमजोर हो जाता है ,तो यह देश के 60% कृषि हिस्से को प्रभावित करता है।
मानसून भारतीय खेती की जीवन रेखा है। इस पर 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर है। जैसा कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति से भी स्पष्ट है कि भारत में मानसून का कितना महत्व है। अगर एक बार भी मानसून खराब रहता है, तो कई राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। चूंकि हमारे यहां जनसंख्या दबाव की वजह से अधिकांश क्षेत्र में खाद्य फसलें ही उगाई जाती हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां फ्लोराइड -आर्सेनिक युक्त जल की समस्या भी गंभीर हो चली है, जो गांवों में के अधिकांश बीमारियों का कारण है। न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादन, जल स्रोतों के सूखने, भूगर्भिक जल स्रोतों पर दबाव से परिस्थितिकी तंत्र में दबाव का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे जैव विविधता पर संकट उत्पन्न होता है और यह जैव विविधता पर बढ़ता दबाव जूनोटिक बीमारियों को फैलने का कारण बनता है।
दूसरी तरफ मानसून के खराब होने से किसानों की आय पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही किसान को कुपोषित जलजनित जूनोटिक बीमारियों से भी खतरा है। इन सब का कारण किसानों की बचत पर पड़ता है। देश के वित्तीय व मानव संसाधन पर निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होंगे ही। मानसूनी वर्षा जब कम होती है, तो किसान खाद, बीज बुवाई-जुताई का खर्च यानी लागत भी नहीं निकाल पाते। आज भी भारत के बहुत से किसान खेती की बुआई के लिए असंगठित क्षेत्रों से ऋण लेते हैं ,क्योंकि यहां आसानी से बिना कुछ जरूरी जमानत के ऋण मिल जाता है, भले ही ब्याज दर बहुत ऊंची रहती है। लागत नहीं निकाल पाने वाले किसान मोटे ऋण को कैसे चुका पायेगा? यह भी सच्चाई है कि किसान को और भी खर्चें उठाने होते हैं ,जैसे- मकान ,शादी-विवाह, बीमारियां इत्यादि। यहां से किसान अपने घरेलू खर्चों के लिए भी कई बार सेठ-साहूकारों के ब्याज जाल में फंस जाते हैं। जब ब्याज चुका नहीं पाते, तो घर में पारिवारिक तनाव, नशे का सेवन तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आती है। गांवों में कृषि पर ज्यादा निर्भरता और मानसून की अनिश्चितता के कारण अकुशल श्रम की फौज तैयार होती हैं, जिनको सामाजिक-आर्थिक दशाओ से जूझना पड़ता है। चूंकि कौशल व शिक्षा के उनके अवसर सीमित होते है, अतः मजबूर होकर शहर में पलायन करते है, जहां झुग्गी बस्तियों में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के गरिमा पूर्ण जीवन के अधिकार के दावों को खोखला साबित करती है।
आंकड़े बताते है कि कृषि का जीडीपी में लगभग 15% योगदान है। सरकारों ने सब्सिडी मुहैया कराने के प्रयास किए जरूर है, लेकिन मानसून की अनिश्चितता में किसान लागत ही निकाल पाने में असमर्थ है। उन पर संस्थागत ऋण को न चुका पाने अथवा एनपीए का खतरा मंडराता है। इस हालात में सरकारें ऋण- माफी की घोषणा करती है , जिससे वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। वहीं अकाल के समय में तो और अधिक दबाव पड़ता है। गांवों की अर्थव्यवस्था चरमर्रा जाने से बाजार में मंदी आ जाती है। इसके कारण बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी होती है, जो लूट-मार और अपराधों को जन्म देती है।
उत्पादन की कमी से मुख्यतः खाद्यान्न व तिलहन की मांग बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ने के पर्याप्त आसार होते है। पूर्ति के लिए विदेशों से आयात करना पड़ेगा ,जिससे भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कम बारिश या अकाल से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी प्रभावित होगा, जो भारत में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक हो जाए तो बाढ़ ,भूस्खलन ,मृदा अपरदन ,पारिस्थितिकी संकट जैसे प्राकृतिक खतरे उत्पन्न हो जाते है, इनसे जान-माल, खेती के नुकसान तथा आधारभूत विकास को खतरा पैदा हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि मानसून का भारतीय कृषि पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए मानसून में थोड़ा-सा भी विचलन देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। इसके लिए ही भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इससे निकलने के लिए सिंचाई तंत्र में पर्याप्त निवेश करने की जरूरत है। हमें स्वचालित सिंचाई पद्धति को हर किसान तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हम छोटी-छोटी नदियों को जोड़कर वर्षा जल को संचित करके भी सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में बढ़ सकते है।
कृषि के बीजों में पर्याप्त अनुसंधान करके उनका ऐसा रूप तैयार किया जाए, जो कम सिंचाई में अधिक उत्पादन दे सके। ऐसे ही अन्य अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाये,जो अधिक उत्पादन में सहायता कर सके। हमें खाद्यान्न फसलों से नगदी फसलों एवं फल-सब्जी के उत्पादन की तरफ भी कदम बढ़ाने चाहिए, जिससे बचत बढ़ सकती है। सरकार को भी कृषि में आधारभूत विकास करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसे सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए,जो किसानों को प्रशिक्षण, कृषि का तकनीकी ज्ञान, कौशल व सब्सिडी देकर उत्पादन की मार्केटिंग कर इस मानसूनी जुए से किसानों को बचा सके। इन प्रयासों से किसानों सक्षम हो सकेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे पाएंगे।
प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है. “भारतीय संस्कृति, समता एवं एकता को बनाते हुए खेती-किसानी के हित में कार्यरत हमारी पूरी टीम किसानो के हित के लिए निष्ठा एवं सम्पूर्ण सेवा भाव से लगी है। कर्प्या लाइक शेयर एवं अपने सुझाव देकर जितना बन सके, सहयोग करें – The Last Yogi”